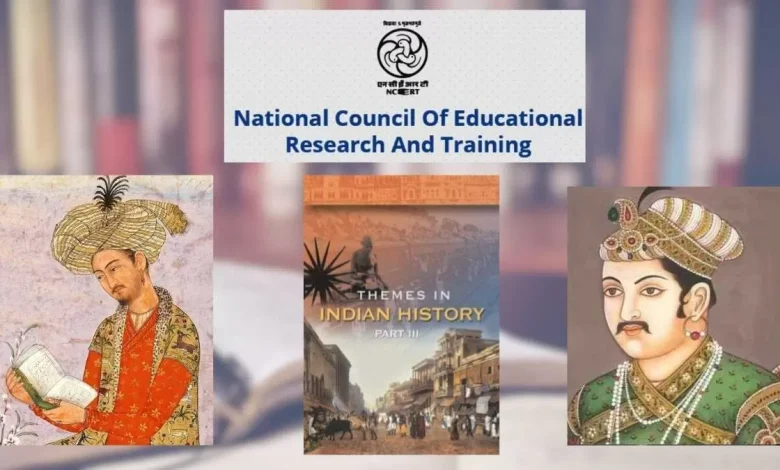
आज के दौर में इतिहास केवल तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं रह गया, बल्कि समाज के सोचने-समझने के तरीके को गढ़ता है। स्कूलों की किताबें जब बदलती हैं, तब उनका असर केवल छात्रों तक नहीं, बल्कि पूरे समाज में छाया महसूस होता है। हालि में एनसीईआरटी इतिहास पुस्तकों में हुए बदलावों ने एक बार फिर यह चर्चा छेड़ दी है कि बच्चों को सचमुच इतिहास से क्या सिखाना चाहिए और किस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनकी बुनियाद को आकार मिलना चाहिए।
कई दशक से भारतीय स्कूलों की इतिहास-पुस्तकों में मुगल साम्राज्य का विशेष स्थान रहा है। बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, सल्तनत-काल से लेकर मुगलिया दौर, हमारे अध्यायों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं कथाओं और सत्ताओं के इर्द-गिर्द घूमता था। कहीं उनका स्थापत्य, उनकी प्रशासन व्यवस्था, कहीं उनकी कला, तो कहीं धर्म और संस्कृति के रंग। इन सबसे एक तसवीर बनती थी मन में दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी के शाही दरबारों की।
लेकिन अब नई किताबों में यह तस्वीर काफी बदल दी गई है। मुगलों के अध्याय संक्षिप्त कर दिए गए हैं, उनके शासन-प्रशासन, स्थापत्य, संगीत, धार्मिक सहिष्णुता की जगह अब संघर्ष, मंदिरों पर हमले, शासन की सख्ती, और उनकी धार्मिक-राजनीतिक नीतियों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। खासतौर पर औरंगजे़ब, बाबर जैसे शासकों को “कठोर” शासक के रूप में सामने रखा गया है।
इतना ही नहीं, इन संशोधनों में एक नया आयाम भी जोड़ा गया है – छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, बाजीराव पेशवा, झाँसी की रानी और सिख, मराठा, राजपूत, विजयनगर साम्राज्य जैसे क्षेत्रीय शासकों को कहीं अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। केवल दिल्ली, आगरा या मुग़ल दरबार नहीं, अब मराठों की गुरिल्ला रणनीति, राजपूतों का संघर्ष, सिख शौर्य, दक्षिण का सांस्कृतिक वैभव, सब अलग-अलग अध्याय में जगह पा रहे हैं।
नई किताबों में अब “डिस्क्लेमर” जैसी सूचनाएँ भी शामिल हैं, जिसमें छात्रों को बताया गया है कि इतिहास की घटनाएँ अपने समय और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में देखनी चाहिए, और आज के समाज या किसी भी समुदाय पर बीते दौर के आधार पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए।
इन बदलावों को लेकर शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी का तर्क है कि, एक तो बच्चों पर पाठ्यक्रम का दिमागी बोझ हल्का करना है। महामारी के बाद यह और ज़रूरी समझा गया। दूसरा, ऐसी भी मंशा है कि इतिहास के बड़े कैनवस पर केवल कुछ वर्णनों तक ही सीमित रहना ठीक नहीं, बल्कि बच्चों को सैकड़ों सालों की जटिलता, विविधता, और क्षेत्रीय समाजों, संघर्षों एवं हर स्तर की उपलब्धियों की समझ भी मिले।
कुछ सामाजिक संगठन वर्षों से यह राय रखते थे कि स्थानीय नायकों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया, जबकि दिल्ली की सल्तनत और मुगलों पर ध्यान रहा। उनका मानना था कि भारत सबसे बड़ा विविधताओं वाला देश है, जिसकी असली शक्ति हजारों छोटे-बड़े राजघरानो, समाज सुधारकों, वीरांगनाओं, कवियों में है। इसी अनुरूप, नई किताबें उन स्थानीय नायकों, उनके संघर्ष, और लोककल्याणकारी प्रयासों को केंद्रीय भूमिका देती दिखती हैं।
वहीं, आलोचकों का आरोप है कि यह परिवर्तन कहीं न कहीं समकालीन राजनीतिक विचारधारा से भी प्रेरित है, जो मुस्लिम शासकों के महिमामंडन की बजाय हिंदू प्रतीकों, मराठा/राजपूत राष्ट्रनायकों के गौरव को उजागर करना चाहती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि माता-पिता, विद्यार्थी, जन प्रतिनिधि और प्रांतों की ओर से, लगातार परिवर्तन मांगने, क्षेत्रीय गौरव की आवश्यकता जताने की आवाज़ें – बीते एक दशक में बहुत तेज़ रही हैं।
इतिहास बदलता नहीं। बल्कि उसका लेखन, उसके विशेष पहलू, समय-समय पर समाज की ज़रूरत के अनुसार प्रमुख या गौण कर दिए जाते हैं। आज के बच्चों के लिए उन्हें उनकी जड़ों की जानकारी देना इतना ही जरूरी है, जितना यह जानना कि भारत पर किसने कब आक्रमण किया या शासन किया।
इस नई प्रस्तुति में आप पाएँगे दिल्ली की बजाय महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, बंगाल के नायक अपने पूरे विस्तार के साथ किताब में हैं। अब मंदिरों, संस्कृति, त्याग, सामाजिक सुधार विद्रोह, महिलाओं, किसानों, संतों, कवियों और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए क्षेत्रीय संघर्षों को भी केंद्रीय महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता या सामंजस्य की छवि की जगह– टकराव, प्रतिरोध, संघर्ष और शासन की सख्ती पर चर्चा अधिक है।
मुग़ल अध्यायों को संक्षिप्त करने के कारण, विद्यार्थियों को मुग़ल काल की स्थापत्य कला, चित्रकला, दरबारी संस्कृति जैसे अध्यायों की जगह अब वह देखेंगे मुग़ल शासकों द्वारा धार्मिक स्थानों पर हमले, जज़िया कर, औरंगज़ेब की नीतियाँ, उनके उत्तराधिकार युद्ध आदि।
आम तौर पर, शिवाजी महाराज को पहले केवल “मराठा शक्ति के स्थापक” के रूप में पढ़ाया जाता था, अब उनकी प्रशासनिक क्षमता, युद्ध शैली, लोककल्याण, और स्वतंत्रता-बोध पर विस्तार किया गया है।
इसी तरह महाराणा प्रताप का नाम और युद्ध पहले संक्षिप्त में आता था, अब उन्हे शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक के रूप में विस्तृत स्थान दिया गया है।सिख गुरु गोविंद सिंह, मराठा पेशवा, छत्तीसगढ़ के वीर, चोल, विजयनगर तथा असम के अहोम शासकों पर छपी नई सामग्री दिखाती है कि पाठों के केंद्र में सिर्फ बड़े साम्राज्य नहीं, बल्कि विमर्श, विविधता और संघर्ष की कहानियाँ हैं।
डिस्क्लेमर भी बदलाव है अब कहा गया है कि इतिहास के “डार्क पीरियड” का संबंध आज की सामाजिक पहचान से जान-बूझकर न जोड़ा जाए।
कई मानते हैं कि इतिहास में क्षेत्रीय संतुलन बच्चों को भारत की विविध सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। हर राज्य के बच्चे अपने-अपने सगे नायकों में प्रेरणा पा सकते हैं, जो पहले शायद किसी एक पेज तक सीमित थे।इसी के साथ, संघर्ष के अध्यायों से बच्चे सीखेंगे कि भारत कोई एक राजवंश या सांस्कृतिक ताकत से नहीं बना, बल्कि सैकड़ों बोलियों, धर्मों, आंदोलनों, कलाकारों और आम लोगों की मेहनत से गढ़ा गया है।
अब बच्चा केवल “दिल्ली विजय” या “सल्तनत का वैभव” ही नहीं पढ़ेगा, बल्कि जाति, धर्म, समाज, भाषा, संस्कृति के बहावों, टकरावों, मेलजोल व लोकप्रिय विद्रोह को समझ सकेगा। परिणामस्वरूप, उसके भीतर सामाजिक समता, प्रश्न करने का विवेक और जड़ों से जुड़ने का गर्व दोनों मजबूत होंगे।
छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, झाँसी की रानी, कुँवर सिंह – ये अब सिर्फ नाम न होकर पुरस्कार या मातृभूमि प्रेम, साहस और नेतृत्व का “रोल मॉडल” बन सकते हैं।
हाल की नई शिक्षा नीति ने “भारतीयता को केंद्र” में रखने, स्नातक स्तर पर क्षेत्रीय इतिहास, सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं की भूमिका बढ़ाने, और बच्चों को केवल रट्टा नहीं, तर्क, शोध और बहस का मौका देने की बात कही है। यदि यही भावना सचमुच किताबों में उतारी गई, तो छात्र केवल “सुनना-समझना” नहीं, बल्कि “सोचना-विवेचन” भी सीखेंगे।
शिक्षक को अब ज्यादा जटिल और बहुरंगी इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि बच्चे “सच” और “गौरव” दोनों के बीच अंतर कर सकें। अभिभावक, समाज और नीति-निर्माता सबको मिलकर देखना होगा कि कहीं कोई इतिहास “भूल या भुलाया हुआ” न रह जाए। बच्चों को केवल किताब पढ़ने के लिए नहीं, सवाल पूछने-मूल्यांकन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए।
इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, वह भविष्य का रचनाकार भी है। एक ऐसी किताब, जिसमें सारे रंग, कठिनाई, उपलब्धि, संगीत, वियोग व संघर्ष शामिल हो – वही बच्चा भविष्य का संतुलित और विवेकशील नागरिक बनता है। नई किताबें केवल अध्याय नहीं बदल रहीं, बल्कि बच्चों की सोच का दायरा भी बदल रही हैं। हमें संवाद, सहिष्णुता, विविधता और आलोचना की गुंजाइश को कभी कम नहीं करना चाहिए।



