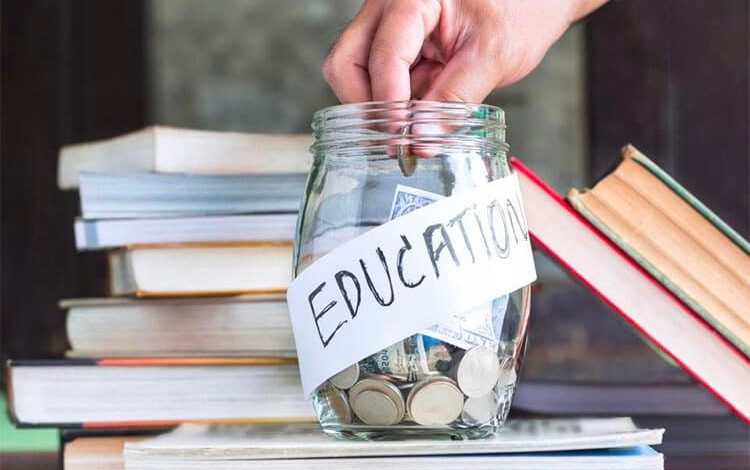
जब कोई छात्र कॉलेज में दाख़िला लेता है, तो वह सिर्फ डिग्री या किताबें नहीं, उस क्लासरूम के साथ भविष्य की उम्मीदें, खुद के पैरों पर खड़े होने का सपना और कई बार पूरे परिवार की मेहनत अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन अब यह सपना पकड़ से दूर होता जा रहा है, क्योंकि स्कूल से निकलते ही छात्रों का पहला सामना होता है कॉलेज की भारी लागत से।
पहले यह सवाल था कि कौन-से कॉलेज में दाख़िला मिलेगा… आज सवाल ये है कि “क्या वह कॉलेज हमारे बजट का हिस्सा बन सकता है?” फीस, किताबें, हॉस्टल, फॉर्म, लैपटॉप, प्रोजेक्ट—हर चीज़ एक नई क़ीमत लिए हुए है।
अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज अब स्मार्ट क्लासरूम, हाई-टेक लैब्स, इंटरनेशनल टाई-अप, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों पर ज़ोर दे रहे हैं। हालांकि यह छात्रों के लिए बेहतर सीखने का माहौल जरूर बनाते हैं, लेकिन इन ढांचागत सुधारों की वित्तीय ज़िम्मेदारी भी उनकी जेब पर पड़ती है।
बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय अब सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। ऐसे में उन्हें ग्लोबल रैंकिंग, फैकल्टी ट्रेनिंग, रिसर्च पब्लिकेशन और फॉरेन एक्सचेंज की दिशा में अधिक निवेश करना पड़ता है, जिसका भार छात्रों से वसूले गए शुल्क से ही संतुलित किया जाता है।
पिछले एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इन संस्थानों का उद्देश्य लाभ कमाना है, जिसकी वजह से शुल्क स्वाभाविक रूप से अधिक रहता है। कई बार तो फीस के अलावा अन्य ‘हिडन कॉस्ट’ जैसे यूनिफॉर्म, लैपटॉप, कोचिंग या परीक्षागत शुल्क भी सिर दर्द बन जाते हैं।
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, हाई-स्पीड इंटरनेट, ई-बुक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी संसाधनों की लागत जितनी लुभावनी दिखती है, उसके पीछे खर्च भी उतना ही होता है। इसका असर भी फीस में झलकता है।
भारत में उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश अब भी जीडीपी का बहुत छोटा हिस्सा है। जबकि कई विकसित देशों में यह खर्च 5–6% तक होता है, भारत में यह आंकड़ा 1% के करीब ही बना हुआ है। यानी खर्च ज़्यादा है, लेकिन अनुदान कम।
अगर फीस बढ़ रही है, तो ये भी देखना होगा कि छात्र को बदले में क्या मिल रहा है।कई प्रमुख संस्थानों ने अब जॉब-ओरिएंटेड, कौशल केंद्रित और उद्योग से जुड़े कोर्स शुरू किए हैं। डेटा साइंस, डिज़ाइन थिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप मैनेजमेंट जैसे विषयों को शामिल किया जा रहा है, जिससे छात्र को सीधे कामकाजी दुनिया से एक्सपोजर मिल सके।
आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केंद्र, और शोध फाउंडेशन के ज़रिए कॉलेज रिसर्च को प्रोमोट कर रहे हैं। नयी योजनाओं में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप शुरू की गई हैं, जिससे छात्रों को आर्थिक मदद के साथ शोध का वातावरण भी मिल रहा है।
नई शिक्षा नीति (2020) और डिजिटल युक्त शिक्षण की वजह से अब गांव-कस्बों में भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच संभव हो रही है। क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन कंटेंट, सामुदायिक लर्निंग सेंटर और मोबाइल क्लासरूम जैसी पहलें इसमें मददगार साबित हो रही हैं।
महामारी के बाद कई विश्वविद्यालयों ने फिजिकल और ऑनलाइन क्लास, दोनों का मिश्रण अपनाया है। इससे उन छात्रों को राहत मिली है जो दूरदराज इलाकों से आते हैं और जिन्हें हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ये जरूर है कि सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनसे फायदा कितना व्यापक हुआ है। शिक्षा की ‘बाजारमूल्यता’ बढ़ी मगर उसमें ‘बराबरी’ आई या नहीं, यह उतना साफ़ नहीं है। फीस बढ़ने के बावजूद कई संस्थानों में शिक्षकों की संख्या घट रही है या फिर अनुभवहीन भर्ती की जा रही है। नई सुविधाओं का लाभ अक्सर शहरी, इंग्लिश मीडियम पृष्ठभूमि वाले छात्रों को ही ज़्यादा मिलता है।ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए एक ही फ़ॉर्म भरना, लोन लेना या स्कॉलरशिप मिलना भी जटिल प्रक्रिया बन जाती है।दूसरे शब्दों में कहें तो, फीस के एवज़ में मिलने वाली सुविधा कुछ छात्रों के लिए लाभकारी है लेकिन अधिकांश के लिए यह उपलब्ध नहीं हो पाती।
2025 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से उच्च शिक्षा को 50,000 करोड़ के आसपास मिला है। प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त फंड मिल रहा है ताकि वो रिसर्च और एक्सीलेंस में अपग्रेड हो सकें।
पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना रिसर्च करने वाले छात्रों को 70,000 रुपये तक की मासिक सहायता। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय योजना ऑनलाइन कोर्सेस को आधिकारिक रूप देना। AI कौशल पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन योजना– जिससे छात्रों को भविष्य-उन्मुख स्किल्स मिलें। शिक्षा ऋण योजनाएं योजना सरकार ने क्रेडिट लिंकेज सिस्टम को बेहतर बनाया है, जिससे बैंक लोन लेना आसान हो सके।
योजनाओं का लाभ लेना शुरू में जितना अच्छा लगता है, ज़मीन पर उस लाभ को पाना उतना आसान नहीं है। ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्र अब भी सिर्फ सरकारी सहायता पर निर्भर रहकर उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं।
देश का युवा आज सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि भविष्य की दिशा का विकल्प ढूंढ रहा है। उसने समझ लिया है कि केवल डिग्री कोई गारंटी नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन की कला, इंटरव्यू की तैयारी, इंटर्नशिप जैसे पहलू अब उतने ही ज़रूरी हो गए हैं जितना की अकादमिक ज्ञान।
कई युवा अब उस कोर्स में निवेश करना चाहते हैं, जो उन्हें वास्तविक अवसर दिला सके, न कि केवल डिग्री का कागज़।”लाखों की फीस देकर अगर फिर भी नौकरी नहीं मिली, तो क्या फायदा?”
इस सोच ने अब कॉलेज के चयन में भी बदलाव किया है। ‘रैंक’ से ज्यादा अब छात्र पूछते हैं—”कहाँ प्लेसमेंट अच्छा है?”, “फैकल्टी कितनी अनुभवी है?” और “क्या वहां छात्र की सोच को सम्मान मिलता है?”
उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत एक सच है। पर यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा अब सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं रही, यह एक व्यापक रूप ले चुकी है। जो सोच में बदलाव, स्किल्स में विस्तार और आत्मनिर्भरता को जन्म देती है।जरूरत है संतुलन की लागत और गुणवत्ता में, संसाधन और समावेशन में, डिजिटल और मानवीय संपर्क में।
सरकार यदि योजनाएं बना रही है, तो संस्थानों को उसकी ईमानदार क्रियान्विति करनी होगी। छात्रों को भी समझदारी से कोर्स और कॉलेज चुनने होंगे। अभिभावकों को सपनों और संसाधनों के बीच सामंजस्य बैठाना होगा।



